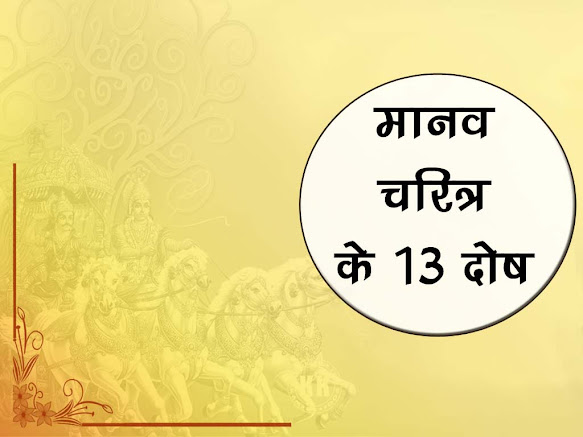मानव चरित्र के तेरह स्वभावगत मूल्यह्रास (मानव चरित्र के प्रमुख दोष एवं उनका निदान)
मानव चरित्र के तेरह स्वभावगत मूल्यह्रास
महाभारत के अनुसार इनमें से तेरह प्रमुख दोषों की कोटि में आते हैं। प्रस्तुत प्रसंग (शान्तिपर्व, अध्याय १६३) में युधिष्ठिर पितामह भीष्म से ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं और पूछते हैं. -
- भरतश्रेष्ठ, परम बुद्धिमान् पितामह ! क्रोध, काम, शोक, मोह, विधित्सा, परासुता, मद, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, निन्दा, दोषदृष्टि, और दैन्य ये सब दोष किससे उत्पन्न होते हैं ?
यतः प्रभवति क्रोधः कामो वा भरतर्षभ।
शोकमोहौ विधित्सा च परासुत्वं तथा मदः ।।
लोभो मात्सर्यमीर्ष्या च कुत्सासूया कृपा तथा ।
एतत् सर्वे महाप्राज्ञ याथातथ्येन मे वद ।।
आइए, जिस तरह हमनें धर्मकाया के गुणों को विस्तार से समझा, उसी तरह पितामह भीष्म से इन दोषों की उत्पत्ति और निदान का मार्ग सीखने का प्रयास करते हैं। भीष्म कहते हैं कि "ये तेरह दोष प्राणियों के अत्यन्त प्रबल शत्रु हैं जो मनुष्य को सदैव चारो ओर से घेरे रहते हैं। मनुष्य के क्षण भर असावधान होते ही ये उस पर भेड़ियों की तरह टूट पड़ते हैं। इन्हीं से सब दुख प्राप्त होते हैं और इन्हीं के वशीभूत हो मनुष्य की पापकर्मों में प्रवृत्ति होती है।"
१. क्रोध :-
- इन तेरह दोषों में सबसे प्रमुख क्रोध है आप जानते हैं कि दुर्योधन ने इसी क्रोध के कारण क्या क्या नहीं किया। हम सभी को छोटी से बड़ी बात पर दिन में बीस बार गुस्सा आता है। फिर कैसे कैसे भाव आते हैं "मैं उसको छोडूंगा नहीं, मैं उसको ठीक कर दूँगा, आदि आदि ।" भीष्म बताते हैं कि "क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है, और दूसरों के दोष देखने से बढ़ता है" - "लोभात् क्रोधः प्रभवति परदोषैरुदीर्यते ।"
- लोभ लालच है – जो है उससे असन्तुष्टि, और जो नहीं है उसे पाने की तृष्णा । - हमारे अन्दर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, महत्वाकांक्षा होती है। नया वाला फोन चाहिए, महँगी वाली ड्रेस चाहिए, बड़ी वाली गाड़ी, घर में ढेर सारे नौकर चाकर, विदेश यात्रा, और पता नहीं क्या क्या चाहिए यही लोभ है। बाजार में इसी अवगुण को गुण के भेष में परोसा जाता है ये दिल मांगे मोर' इसी लोभ का परिष्कृत रूप है महत्वाकांक्षा अंग्रेज़ी में इसे ऐम्बिशन कहते हैं। आधुनिक विचारकों के मतानुसार यदि व्यक्ति में ऐम्बिशन नहीं है, तो उसका जीवन व्यर्थ है ।
- इसीलिए आगे चल कर डॉक्टर बनना है, डी. एम. बनना है, एम.एल.ए., एम.पी., मन्त्री, प्रधानमन्त्री, और जाने क्या क्या बनना है। बस इसी गाड़ी में बैठा इक्कीसवीं सदी का मानव मन चौबीस घन्टे घूमता रहता है। और यदि गाड़ी पंक्चर हो गयी, किसी ने ब्रेक लगा दिया तो पिताजी ने फोन के लिए पैसे नहीं दिए, दोस्त ने उधार नहीं दिए, माताजी ने स्वछन्द घूमने फिरने या शराब - सिगरेट पीने पर खरीखोटी सुना दी, आइ. आइ.टी. या आइ. ए. एस. की परीक्षा में ठीकठाक नम्बर नहीं आए, शहर वालों ने चुनाव में वोट नहीं दिए, तो । बस फिर क्या है खून खौल उठता है, सारे शरीर में आग लग - जाती है। लोभ की सन्तुष्टि न होने पर क्रोध आता है।
- ऊपर से चारों तरफ बुराइयाँ ही बुराइयाँ, कमियाँ ही कमियाँ नज़र आती हैं। बाबू - अफसर - राजनेता सभी भ्रष्ट हैं, प्रधानमन्त्री को देश चलाना नहीं आता, सचिन तेन्दुलकर को बैटिंग करनी नहीं आती- वर्ल्डकप हरवा दिया, रामसिंह के लड़के को गणित नहीं आती घूस देकर इन्जीनियर बन गया। ऐसा ज़माना देखकर गुस्सा तो आयेगा ही। भीष्म कहते हैं, "दूसरों के दोष देखने पर क्रोध बढ़ता है।"
- यह जो बारबार खून खौलता है, इससे बचने का उपाय क्या है ? भीष्म की सीख है कि क्षमा ही एकमात्र रास्ता है। क्षमा से ही क्रोध शान्त होता है, क्षमा से ही उससे जड़ से छुटकारा मिलता है। क्षमया तिष्ठते राजन् क्षमया विनिवर्तते।"
- लेकिन क्षमा करने के लिए कोई स्विच या बटन तो है नहीं कि दबाते ही शुरू हो जाय या बन्द हो जाय क्षमा के क्रियान्वयन के पहले एक लम्बी तैयारी होनी चाहिए। क्षमा क्यों करें, इसका उत्तर तलाशना पड़ेगा। इस बात का बोध होना होगा, कि जिस व्यक्ति या व्यवस्था पर हमें क्रोध आ रहा है वह अज्ञानी है, या अज्ञान से उपजी और अज्ञान में स्थित है। ऐसे में व्यक्ति या व्यवस्था के लिए करुणा उत्पन्न होती है, क्रोध नहीं। फिर जो इच्छा पूरी नहीं हो रही है, वह मूर्खतापूर्ण इच्छा है, इस बात का अहसास हो । वास्तव में मूर्खों के पास ही इच्छाएं होती हैं, ज्ञानी पुरुष इच्छाओं से मुक्त होता है।
- एक और महत्वपूर्ण बात जो हमने पहले देखी है, वह यह कि धर्म के अभाव में ही अधर्म का अस्तित्व है, और धर्म के बढ़ने से ही अधर्म क्षीण होना शुरू होता है। धर्म की प्रारम्भिक उपस्थिति में भी इतना तो बोध होने ही लगता है कि जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसके पीछे अनुमन्ता ईश्वर की अनुमति है, या फिर हमारी न समझ में आने वाली उसकी लीला है। इतनी भूमि तैयार हो तो क्षमा के अंकुर फूट सकते हैं। क्षमा करुणा की सहोदरी है, धर्म के मूल में है, धर्मशील व्यक्ति के आचार की सुगन्ध है। क्षमा की क्षमता के लिए धर्म साधना होगा। परन्तु साथ में बुद्धि और विवेक भी चाहिए, नहीं तो हम आन्दोलन करने लगेंगे कि रावण को, कंस को दुर्योधन को, महिषासुर को सभी को क्षमादान मिलना चाहिए। यहाँ यह भी ध्यान देना होगा कि भीष्म के अनुसार क्षमा में क्रोध का शमन है, पाप और पापाचारियों का नहीं।
२. काम :-
संकल्पाज्जायते कामः सेव्यमानो विवर्धते ।
यदा प्राज्ञो विरमते तदा सद्यः प्रणश्यति ।।
- "काम संकल्प से उत्पन्न होता है। उसका सेवन किया जाय तो बढ़ता है। जब बुद्धिमान पुरुष उससे विरक्त हो जाता है, तब वह (काम) तत्काल नष्ट हो जाता है।"
- थोड़ा गूढ़ विषय है। एक ओर काम को चार पुरुषार्थों में रखा गया है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उसका साकार रूप कामदेव देवता हैं, कोई असुर या राक्षस नहीं । फिर भगवान शिव उसे भस्म कर डालते हैं। पुनः शिव की ही कृपा से वह कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। काम के बिना सन्तानोत्पत्ति सम्भव नहीं है। भोग विलास की वस्तुएं बननी बन्द हो जाय, तो दुनिया में व्यापार ही बन्द हो जायेगा।
- फिर कामाग्नि या कामातुर जैसे शब्दों का प्रयोग, यथा कामातुराणां न भयं न लज्जा', उसके निषेध की ओर इंगित करता है। पशुओं में मनुष्य जैसा संयम नही है, इसलिए उनमें कामाग्नि की तीव्रता प्रत्यक्ष परिलक्षित होती है। काम के केन्द्र में भले ही नर-मादा सम्बन्ध हों, परन्तु उसका विस्तार व्यापक भोगविलास में दिखता है। विलासिता का जीवन प्रायः अधोगामी होता है। आपने नशेड़ियों, शराबियों की दुर्गति देखी है; किस तरह वे नालियों में चेतनाहीन पड़े पाये जाते हैं। भोगविलास में फँसा व्यक्ति न तो अपने स्वयं के कल्याण के बारे में सोच सकता है, और न ही अपने परिवार या समाज के उत्थान के बारे में। इसीलिए संयम से स्वतन्त्र हो जाने पर काम मनुष्य के लिए अतिशय दुखदायी दोष साबित होता है।
- काम की उत्पत्ति संकल्प में है। जब हम ठान लेते हैं कि हमें तो यह करना ही है, हमें तो यह पाना ही है, तो वहीं काम का जन्म होता है। जितना अधिक उसका सेवन किया जाता है, उतना ही अधिक वह बढ़ता है, ठीक जैसे घी डालने से अग्नि की ज्वाला बढ़ती है।
- पितामह भीष्म कहते हैं कि विरक्ति ही इससे छुटकारा पाने का एकमात्र मार्ग है। जो मिला है, वह ईश्वर प्रदत्त प्रसाद है। उससे अधिक पाने की इच्छा प्रसाद तो नहीं हो सकती। सारी इच्छाओं, कामनाओं से विरक्ति बुद्धि के जागृत हुए बिना सम्भव नहीं है। और बुद्धि, विवेक, ज्ञान के लिए धर्म के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है।
३. परासुता या पराऽसूया ( डाह, द्रोह, विरोध, शत्रुता का भाव ) :-
परासुता क्रोधलोभादभ्यासाच्च प्रवर्तते ।
दयया सर्वभूतानां निर्वेदात् सा निवर्तते।
अवद्यदर्शनादेति तत्त्वज्ञानाच्च धीमताम्।।
क्रोध, लोभ तथा अभ्यास से परासुता प्रकट होती है। सम्पूर्ण प्राणियों के प्रति दया से और वैराग्य से वह निवृत्त होती है। परदोष-दर्शन से इसकी उत्पत्ति होती है, और बुद्धिमानों के तत्वज्ञान से वह नष्ट हो जाती है ।"
- धर्मशील व्यक्ति सभी प्राणियों को अपना आत्मनि, समझता है। धर्म के अभाव में इसकी विपरीत अवस्था होती है, जिसमें सभी पराये या दूसरे प्रतीत होते हैं। इतना ही नहीं, इन दूसरों के प्रति द्रोह, डाह, विरोध और शत्रुता का भाव होता है। हमारा सारा ध्यान विरोधियों के दोषों की व्याख्या, परदोष-दर्शन में ही रहता है। इसका उदाहरण राजनीति करने वालों में प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसी आग में हम दिनरात झुलसते हुए मरते रहते हैं। निदान का मार्ग है कि सभी प्राणियों के प्रति दया हो, करुणा हो, तो शान्त स्थिर चित्त में इस दोष से मुक्ति मिल जाती है।
४. मोह
अज्ञानप्रभवो मोहः पापभ्यासात प्रवर्तते
यदा प्राज्ञेषु रमते तदा सद्यः प्रणश्यति ।।
"मोह अज्ञान से उत्पन्न होता है, तथा पाप के अभ्यास (बारबार करने) से बढ़ता है। जब मनुष्य विद्वानों में अनुराग करता है, तब उसका मोह तत्काल नष्ट हो जाता है।"
- किसी व्यक्ति या वस्तु से अतिशय अनुराग ही मोह है। धृतराष्ट्र का दुर्योधन के प्रति मोह ही अन्ततोगत्वा पिता-पुत्र दोनों के विनाश का कारण बनता है। पुत्र प्रेम में पिता पुत्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। मोह में वह पुत्र के सभी अनीतिपूर्ण कार्यों में उसका सहयोग करता है। मोह अज्ञान से उपजा अतिकष्टदायी कठोर बन्धन है। क्षणभंगुर, अनित्य वस्तु का अटूट सानिध्य पाने की इच्छा, घोर मूर्खता, दुर्दम अज्ञान नहीं तो और क्या है? अधर्म का निदान धर्म में है। अज्ञान का निदान ज्ञान में है। मरणधर्मा वस्तु का चिरस्थायी साथ स्वयं में विरोधाभास है। ज्ञान, विवेक या सत्य- दर्शन सभी लोकों की वस्तुओं को उनके वास्तविक स्वरूप में देख पाना है। यह दृष्टि आते ही अन्धकार रूपी अज्ञान और मूर्खता नष्ट होना प्रारम्भ हो जाते हैं।
५. विधित्सा ( आयोजन, प्रयोजन सम्पन्न करने की इच्छा ) :-
विरुद्धानीह शास्त्राणि ये पश्यन्ति कुरूद्वह ।
विधित्सा जायते तेषां तत्त्वज्ञानान्निवर्तते ।।
- "कुरुश्रेष्ठ ! जो लोग धर्म के विरोधी (अथवा परस्पर विरोधी) शास्त्रों का अवलोकन करते हैं, उनके मन में अनेकानेक आयोजन सम्पन्न करने की इच्छा रूपी विधित्सा उत्पन्न होती है। यह तत्त्वज्ञान से निवृत होती है। "
- हम सभी के व्यक्तित्व में एक दोष प्रायः देखने को मिलता है। हमारी समस्या यह होती है कि हमें पता नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। हम कभी पिताजी की राय लेते हैं, तो कभी दोस्तों की; वहाँ से बात नहीं बनती, तो पत्र - पत्रिकाओं में चिट्ठी लिखकर पूछते हैं, या फिर कैरियर काउन्सलर की शरण में जाते हैं। बच्चा बीमार हुआ तो पता नहीं कि अंग्रेजी डॉक्टर के पास जायें या होम्योपैथी या आयुर्वेद वाले के पास पड़ोसन कहती है कि बच्चे के ऊपर काला साया है, ओझा को दिखाना होगा। पण्डित जी बता रहे हैं कि शनि और राहु की दशा चल रही है। बड़ी मुसीबत है, अब करें तो क्या करें? फिर तरह तरह के प्रयोजन करने की इच्छा उत्पन्न होती है। हनुमानजी का व्रत भी कर लेते हैं, सत्यनारायण जी की कथा भी करवा देते हैं, ओझा को दिखा ही लेते हैं, और डॉक्टर साहब की दवाई तो चलेगी ही।
- इसी स्थिति को विधित्सा कहते हैं। भीष्म कहते हैं कि परस्पर विरोधी शास्त्रों का अवलोकन करने से यह स्थिति उत्पन्न होती है। या यूँ समझिए कि कई लोगों की राय लेने से। ऐसा दिग्भ्रमित मन केवल तत्त्वज्ञान से रोशनी पाकर शान्त हो सकता है। पर तत्त्वज्ञान मिलेगा कहाँ ? धर्म में केवल धर्मशील व्यक्ति में तत्त्वज्ञान का प्रादुर्भाव सम्भव है।
६. शोक -
प्रीत्या शोकः प्रभवति वियोगात् तस्य देहिनः |
यदा निरर्थकं वेत्ति तदा सद्यः प्रणश्यति ।।
- "जिस पर प्रेम हो, उस प्राणी के वियोग से शोक प्रकट होता है। परन्तु जब मनुष्य यह समझ ले कि शोक व्यर्थ है, उससे कोई लाभ नहीं है, तो उस शोक की शान्ति हो जाती है।"
- प्रियतम के विछोह में शोक का कारण छुपा है। विछोह कई प्रकार से हो सकता है। मृत्यु इनमें से एक है। सम्बन्ध विच्छेद दूसरा प्रकार है। परन्तु शोक की पीड़ा दोनों में एक ही जैसी है। विवेक ही हमें दिखा सकता है कि हर शोक निरर्थक है। इस संसार में जहाँ सभी कुछ नश्वर है, वहाँ कितनी देर या कितनी दूर तक किसी का साथ सम्भव है? एक न एक दिन तो इस संसार का स्वप्न टूटना ही है। स्वप्न तो लगातार बदलता है, और लगातार कुछ न कुछ छूटता जाता है, विस्मृत होता जाता है। फिर एक दिन नींद टूटती है, और स्वप्न - लीला की इति हो जाती है। सोचने में यह सब कुछ कितना सरल, कितना स्पष्ट दिखता है। लेकिन सोचना, विचारना बोध नहीं है। बोध तो सत्य का शाश्वत सानिध्य है। बोध ही तो गौतम को बुद्ध बनाता है। दर्शन शास्त्र के सिद्धान्तों की समझ आपको दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर बना सकती है, बुद्ध नहीं। उसके लिए तो धर्म, ईश्वर और गुरु की शरण लेनी होगी। आराध्य के चरणों में ही इस विवेक का प्रादुर्भाव और इस असाध्य कष्टकारी शोक से छुटकारा सम्भव है।
७. मात्सर्य :-
सत्यत्यागात् तु मात्सर्यमहितानां च सेवया ।
एतत् तु क्षीयते तात साधूनामुपसेवनात्।।
- "सत्य का त्याग और दुष्टों का साथ करने (अहितकारी प्रवृत्तियों के सेवन) से मात्सर्य दोष की उत्पत्ति होती है तात ! श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा और संगति करने से उसका नाश हो जाता है।"
- मात्सर्य मूलतः विद्वेष है। किसी भी प्रकार के विद्वेष के पीछे ईर्ष्या, डाह और असूया होती है, इसलिए इन अर्थों में भी मात्सर्य का प्रयोग देखा जाता है। भीष्म दो तरह से मात्सर्य का कारण देखते हैं। पहला कारण सत्य का त्याग है। कई बार बहुत पढ़े लिखे लोगों से सुनने को मिल जाता है कि गीता, भागवत, विवेकानन्द, गाँधी पढ़ने और बहस करने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन दैनिक जीवन में व्यावहारिक नहीं हैं। दैनिक जीवन में तो झूठ बोलना ही पड़ता है; चोरी भी करनी पड़ती है - चाहे बिजली या टैक्स की चोरी हो, चाहे परीक्षा में नकल करना; फिर रिश्वत भी खिलानी पड़ती है, नहीं तो दफ्तर वाले फाइल ही नहीं बढ़ने देते। यह भाव ही शुद्ध अर्थों में सत्य का त्याग है।
- मात्सर्य का दूसरा कारण है, अहितकारी प्रवृत्तियों की सेवा या सेवन । यह जानने के लिए हमारे लिए क्या हितकारी हैं, क्या अहितकारी, केवल सामान्य बुद्धि पर्याप्त है, किसी विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। नशा करना, लड़ाई झगड़ा करना, किसी की जेब काटना, कहाँ से हितकारी है, कौन से शरीर और मन के लिए स्वास्थ्यवर्धक है? और जो हितकारी नहीं है, वह अहितकारी ही हुआ। फिर भी हमने ऐसी कितनी ही प्रवृत्तियों की आदत डाल रखी है। फिर तो विद्वेष होगा ही - एक दो से नहीं, सभी से। किसी के अच्छे कपड़े देखे, ठाट देखे, किसी की ऊँची पद-प्रतिष्ठा देखी, तो यही भाव पैदा होता है कि लो, ये तो मुझसे भी बड़ा चोर निकला।
- भीष्म कहते हैं कि मात्सर्य से छुटकारा पाने का उपाय है कि श्रेष्ठ जनों की, साधु-सन्तों की संगत की जाय। इनके पास न तो चोरी का माल है, न ही इनके साथ रहने में अपने ठगे जाने का कोई खतरा । फिर इनसे विद्वेष का कोई आधार ही नहीं है। इनके साथ विद्वेष का भाव ही नहीं उठता। धीरे धीरे निर्विद्वेष रहने में आनन्द मिलने लगता है, सुख प्राप्त होता है, और हम मात्सर्य से मुक्त होने लगते हैं।
८. मद:-
कुलाज्ज्ञानात् तथैश्वर्यान्मदो भवति देहिनाम् ।
एभिरेव तु विज्ञातैः स च सद्यः प्रणश्यति ।।
- "अपने उत्तम कुल, उत्कृष्ट ज्ञान तथा ऐश्वर्य का अभिमान होने से देहाभिमानी मनुष्यों पर मद सवार हो जाता है। परन्तु इनके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर वह मद तत्काल उतर जाता है।"
- उत्तम कुल, उत्कृष्ट ज्ञान तथा ऐश्वर्य तो राम और कृष्ण के पास भी था, और रावण और कंस के पास भी। फिर इनमें इतना अन्तर कहाँ से आया? इस प्रश्न का उत्तर इस श्लोक के एक शब्द 'देहिनाम्' (िहन्दी अनुवाद मे 'देहाभिमानी') में मिलता है | जब तक हम अपने को प्रमुख रूप से शरीर या देह समझते हैं, तब तक ही हमें भौतिक लोक में परिभाषित अपने अस्तित्व पर अभिमान होता है। राम अयोध्या नरेश की पदवी से बहुत ऊपर मर्यादापुरुषोत्तम भगवान हैं। कृष्ण मथुरा नरेश या द्वारकाधीश तक सीमित नहीं हैं। उनके सम्बोधन पर गीता श्रीभगवानुवाच' लिखती है। लेकिन रावण और कंस का लंकापति और मथुराधिपति के अतिरिक्त भी कोई अस्तित्व है, इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं मिलती।
- धर्मशील व्यक्ति आत्मा में स्थित है। उसके मानसिक, प्राणिक और दैहिक रूप उसकी छायायें हैं, उसका स्वरूप नहीं। विवेक और बुद्धि से पूर्ण पुरुष को छायारूपी संदिग्ध अस्तित्व पर कभी अभिमान नहीं हो सकता। यह अभिमान तो रस्सी को सर्प समझने के भ्रम से उत्पन्न होता है, अपने कुल, ज्ञान और ऐश्वर्य को अपना स्वरूप मानने से होता है। जब इन तीनों का यथार्थ ज्ञान हो जाय, जब यह समझ में आ जाय कि ये तीनों तो प्रकृति या माया प्रदत्त हैं, तो इनके कारण उत्पन्न मद स्वतः समाप्त हो जाता है।
६. ईर्ष्या :-
ईर्ष्या कामात् प्रभवति संहर्षाच्चौव जायते ।
इतरेषां तु सत्त्वानां प्रज्ञया सा प्रणश्यति।।
"मन में कामना होने से तथा दूसरे प्राणियों की हँसी-खुशी देखने से ईर्ष्या की उत्पत्ति होती है तथा विवेकशील बुद्धि के द्वारा उसका नाश होता है "
मन में जब काम उठता है, भोग-विलास की कामना जगती है, तो अड़ोस पड़ोस में अन्य लोगों की विलासिता की सामग्री पर भी ध्यान जाता है। हमने नये कपड़े खरीदे, तो सभी के नये कपड़ों पर नज़र जाती है। फिर जिनके पास हमसे अधिक अच्छा है, उनसे ईर्ष्या होना स्वाभाविक है। हमारे साथी को दस लाख का पैकेज मिल गया, और हमें चपरासी की भी नौकरी नहीं मिल रही तो समाज के इन जुगाडू सफल लोगों से ईर्ष्या तो होगी ही। भीष्म हों या कोई अन्य महात्मा, सब एक ही बात दोहराते हैं "विवेकशील बुद्धि के द्वारा उसका नाश होता है।" और हम भी वही एक प्रश्न दोहराते हैं - "यह मिलेगी कहाँ ?" "बुद्धं शरणं गच्छामि । धम्मं शरणं गच्छामि । संघं शरणं गच्छामि।" -
१०. कुत्सा ( निन्दा ):-
विभ्रमाल्लोकबाह्यानां द्वैष्यैर्वाक्यैरसम्मतैः ।
कुत्सा संजायते राजन् लोकान् प्रेक्ष्याभिशाम्यति ।।
- "राजन ! समाज से बहिष्कृत हुए नीच मनुष्यों के दोषपूर्ण तथा अप्रामाणिक वचनों को सुनकर भ्रम में पड़ जाने से निन्दा करने की आदत होती है। परन्तु श्रेष्ठ पुरुषों को देखने से वह शान्त हो जाती है।"
- अखबार, टीवी, बाजार, पॉलिटिक्स हर जगह आदमी यही बोलता है, "हमारी - पार्टी अच्छी है, हमारा माल अच्छा है। दूसरे की पार्टी भ्रष्ट है, उसका माल घटिया है ।" हम दिन भर यही सुनते हैं, और धीरे धीरे इसी रंग में रंग जाते हैं। श्रेष्ठ पुरुषों की संगत कीजिए, निन्दा करने की निरर्थक, मूर्खतापूर्ण आदत छूट जायेगी।
११. असूया:-
प्रतिकर्तुं न शक्ता ये बलस्थायापकारिणे ।
असूया जायते तीव्रा कारुण्याद् विनिवर्तते ।।
- "जो लोग अपनी बुराई करने वाले बलवान् मनुष्य से बदला लेने में असमर्थ होते हैं, उनके हृदय में तीव्र असूया (दोषदर्शन की प्रवृत्ति) पैदा होती है, परन्तु दया का भाव जाग्रत् होने से उसकी निवृत्ति हो जाती है। #
- हम दोष उन्हीं में ढूढ़ते हैं, जिनका हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और जब हम कुछ नहीं कर सकते, तो नफरत तो कर ही सकते हैं, उनकी निन्दा करके उनका मान घटाने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। यही असूया है। जब समझ में आता है कि यहाँ सब दुखी हैं, सब किसी न किसी रूप में पीड़ित हैं 'अनित्यं असुखं लोकं इमम्।' - तब सभी प्राणियों के लिए करुणा का भाव उत्पन्न होता है। करुणा में ही असूया का निदान है।
१२. कृपा :-
- कृपणान् सततं दृष्ट्वा ततः संजायते कृपा धर्मनिष्ठां यदा वेत्ति तदा शाम्यति सा कृपा ।। "सदा कृपणों को देखने से अपने में भी दैन्यभाव पैदा होता है। धर्मनिष्ठ पुरुषों के उदार भाव को जान लेने पर वह दैन्यभाव नष्ट हो जाता है "
- कृपा का अर्थ यहाँ तरस खाने से है। "हाय राम ! उसके पास तो यह भी नहीं है, वह भी नहीं है, बेचारा कैसे गुजर बसर करता होगा।" फिर ऐसे बेचारों को देखते देखते अपने ऊपर भी तरस आने लगता है । "हाय ! मैं भी तो कितना गरीब हूँ, मेरे पास भी तो कुछ नहीं है।" धर्मनिष्ठ व्यक्ति का भाव ठीक इसके विपरीत होता है। वह तो कहता है 'अहं ब्रह्मास्मि "शिवोऽहम् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् । जो परमेश्वर को जानता हो, जो ब्रह्म हो, शिव हो, उसे तीनों लोकों में क्या है जो प्राप्त नहीं है। जिसके पास सब कुछ हो, वह केवल दे सकता है, ले नहीं सकता। ऐसे धर्मनिष्ठ पुरुषों का सत्संग करने से कृपणता का दैन्य भाव समाप्त हो जाता है।
१३. लोभ :-
- अज्ञानप्रभवो लोभो भूतानां दृश्यते सदा अस्थिरत्वं च भोगानां दृ ष्ट्वा ज्ञात्वा निवर्तते ।। "प्राणियों का भोगों के प्रति जो लोभ देखा जाता है, वह अज्ञान के ही कारण है। भोगों की क्षणभंगुरता को देखने और जानने से उसकी निवृत्ति हो जाती है ।"
- अज्ञान में ही सभी प्रकार के लोभों की उत्पत्ति है। अगर मुझे ये मिल जाय, अगर मैं वो बन जाऊँ, तो मेरे सभी दुखों का अन्त हो जायेगा, और मैं बहुत सुखी हो जाऊँगा । ऐसा सोचना घोर अज्ञान नहीं तो और क्या है? यह जान लेने पर कि सभी के सभी भोग अस्थिर हैं, कुछ भी बहुत देर तक टिकने वाला नहीं है, वस्तुओं के प्रति लोभ या उन्हें प्राप्त करने की इच्छा समाप्त हो जाती है।
इन तेरह दोषों के वर्णन के पश्चात इस अध्याय में पितामह भीष्म का अन्तिम वचन अत्यन्त महत्वपूर्ण है-
एतान्येव जितान्याहुः प्रशमाच्च त्रयोदश ।
एते हि धार्तराष्ट्राणां सर्वे दोषास्त्रयोदश ।।
त्वया सत्यार्थिना नित्यं विजिता ज्येष्ठसेवनात् ।।
"कहते हैं, ये तेरहों दोष शान्ति धारण करने से जीत लिए जाते हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों में ये सभी दोष मौजूद थे और तुम सत्य को ग्रहण करना चाहते हो, इस लिए तुमने श्रेष्ठ पुरुषों के सेवन से इन पर विजय प्राप्त कर ली "
धृतराष्ट्र एवं दुर्योधन का चरित्र समाज की पतनोन्मुखी गति का परिचायक है। उनके भीतर विद्यमान यही तेरह दोष समाज में व्याप्त मूल्यों के ह्रास को लक्षण और कारण हैं। हमने देखा कि धर्म की अनुपस्थिति ही अधर्म का अभ्युदय है, मूल्यों का ह्रास है। धर्म की पुनर्स्थापना ही इसका निदान है। भीष्म के अनुसार क्षमा, विरक्ति, प्रज्ञा, बुद्धि, महात्माओं के दर्शन और उनके सानिध्य में ही इन सभी दोषों का निदान है।