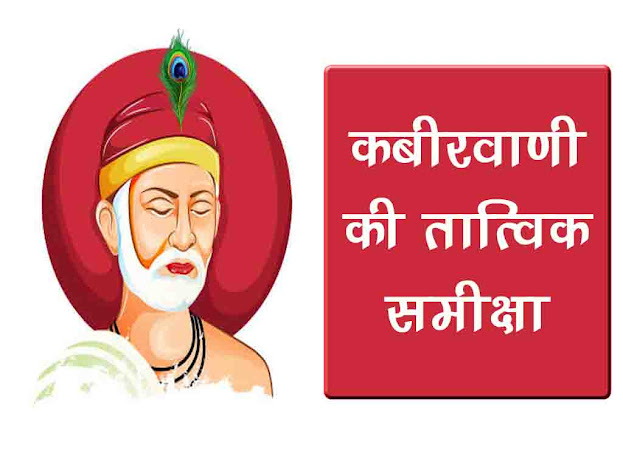कबीरवाणी की तात्विक समीक्षा
कबीरवाणी की तात्विक समीक्षा -प्रस्तावना ( Introduction)
मध्यकाल के हिन्दी कवियों
की रचनाओं के प्रमाणिक पाठ की समस्या बहुत उलझी हुई है और कबीर जैसे फक्कड़ संत के
सम्बन्ध में, जो ‘पुस्तक देहु बहाइ' का उपदेश देते रहे, यह समस्या और भी
उग्र रूप धारण कर लेती है। कबीर पर शोधकार्य करते समय विभिन्न हस्तलिखित तथा
मुद्रित प्रतियों में कुल मिलाकर लगभग सोलह सौ पद, साढ़े चार हजार साखियाँ
और एक सौ चौंतीस रमैनियाँ मिली हैं। पदों, साखियों तथा रमैनियों के
अतिरिक्त भी सौ रचनाएँ, भिन्न-भिन्न ग्रन्थों के रूप में, ऐसी और प्राप्त
होती हैं जिन्हें कबीरकृत कहा जाता है। अगर और खोज की जाए तो इनकी संख्या में
वृद्धि ही होती जाएगी। कबीरपंथियों का तो विश्वास है कि सद्गुरु कबीर की वाणी अनंत
है, उसकी संख्या का अनुमान वनस्पति- समुदाय के पत्तों और गंगा
के बालुका- कणों से लगाया जा सकता है-
जेते पत्र बनस्पती, औ गंगा की रैन ।
पंडित बिचारा क्या कहै
कबीर कही मुख बैन ॥
कबीरवाणी की तात्विक समीक्षा
➽ ऐसा अंश जो समस्त
प्रतियों में समान रूप से मिलता हो, सुगमता से प्रामाणिक माना
जा सकता है, किन्तु कबीर के सम्बन्ध में यह स्थिति कुछ विलक्षण है। एक
भी पद ऐसा नहीं है जो सभी प्रतियों में समान रूप से मिलता हो, साखी केवल एक है
जो सभी प्रतियों में मिलती है और रमैनी भी ऐसी कोई नहीं जो सभी प्रतियों में मिलती
हो । प्रति भी ऐसी कोई नहीं मिलती जो कबीर के जीवन काल की हो अथवा जिसकी परंपरा ही
इतनी प्राचीन हो कि उसे निरापद रूप से कबीर के जीवन काल का माना जा सके।
पाठ-विकृतियाँ भी सभी प्रतियों में मिलती हैं। इस स्थिति में दावे के साथ यह कहना
कठिन है कि कबीर की रचना कितनी और किस रूप में प्रमाणिक है। उनके कंठ से जो कुछ
निकला वह वायु में विलीन हो गया; उसे न तो किसी यंत्र में बाँधा गया और न ही
तुरन्त लिपिबद्ध किया गया।
➽ यदि कोई ऐसा वैज्ञानिक
आविष्कार हो जाए जिसके द्वारा शताब्दियों पूर्व किसी व्यक्ति के मुख से निकले हुए
शब्द पुनः यथावत् उपस्थित किए जा सकें तभी पूर्ण निश्चय के साथ कबीर की वाणी का
प्रमाणिकतम रूप स्थिर किया जा सकता है। उसके अभाव में दूसरा निरापद मार्ग है पाठ
सम्पादन के मान्य सिद्धान्तों के आधार पर समस्त उपलब्ध सामग्री का तुलनात्मक
अध्ययन कर उनका पारस्परिक सम्बन्ध स्थिर करना और तब उसकी सहायता से ऐसा पाठ
निर्धारित करना जिसे यत्किंचित् मतवैभिन्य होते हुए भी सभी पूर्ववर्ती पाठों से
प्राचीनतर अथवा दूसरे शब्दों में प्राचीनतम तथा प्रमाणिकतम माना जा सके। काल के
स्थूल आवरण को भेदकर आलोच्य रचना के शताब्दियों पूर्व रूप तक पहुँचने का यही एक
निरापद मार्ग है। संयोगवश यह प्रक्रिया मन की उस उल्टी साधना से मिलती है जिसका
उपदेश सन्तों ने दिया और जिसे उन्होंने अपनी करनी में भी उतारा। कबीर का कथन है-
मन कै मतै न चालिए, छांड़ि जीव की बांनि ।
ताकू केरा तार ज्यौं, उलटि अपूठा आंनि ॥ - क. ग्रं., साखी 29-23
➽ यही सिद्धान्त पाठ
-निर्धारण में भी सहायक होता है। उपलब्ध प्रतियों के वर्तमान साक्ष्यों को आँख
मूँदकर मान लेने की 'बानि' अच्छी नहीं होती, बल्कि 'अपूठा' (उल्टा) चलकर उनके
पूर्व रूप की खोज करने में ही उनकी सहायता लेनी चाहिए।
➽ कबीर वाणी की विषम पाठ
समस्या को सुलझाने के लिए जो प्रक्रिया अपनायी गयी है उसे पाठ-सम्पादन की
पारिभाषिक शब्दावली में कहा जा सकता है कि पहले विभिन्न प्रतियों का परीक्षण और
फिर उनका पारस्परिक पाठ- मिलान कर अत्यन्त सतर्कतापूर्वक निर्धारित समस्त 'निश्चेष्ट' तथा 'सचेष्ट' पाठ विकृतियों की
सहायता से उनका पाठ सम्बन्ध निर्धारित किया गया है और तदनंतर केवल उन्हीं रचनाओं
को कबीरकृत स्वीकृत किया गया है जो किन्हीं भी दो या अधिक ऐसी प्रतियों में मिलती
हैं जिनमें किसी प्रकार का संकीर्ण सम्बन्ध' नहीं है, अर्थात् जिनमें
पाठ सम्बन्धी ऐसी विकृतियाँ (जानबूझकर अथवा अनजान में की हुई) समान रूप से नहीं
पाई जातीं जिनका आविर्भाव कवि के मूल पाठ का परवर्ती सिद्ध होता हो और इसी आधार पर
उन रचनाओं का पाठ भी निर्धारित किया गया है।
➽ इस प्रकार उपलब्ध सामग्री में से कबीर की प्रमाणिक रचना के रूप में दो सौ पद या शब्द, बीस रमैनियाँ, एक चौंतीसी रमैनी तथा साढ़े सात सौ के लगभग साखियाँ प्राप्त होती हैं।
➽ यहां प्रस्तुत कबीरवाणी
का पाठ इतः पूर्व सभी संस्करणों से अधिक विश्वसनीय है यह बात दो-चार स्थूल
उदाहरणों से अधिक स्पष्ट हो सकेगी। कबीर का एक पद 'कबीर ग्रंथावली' में इस प्रकार है-
मेरी मेरी करता जनम गयौ ।
जनम गयौ परि हरि न कह्यौ ॥ टेक ॥
बारह बरस बालपन खोयौ बीस बरस कछु तप न कियौ ।
तीस बरस तैं राम न सुमिरयौ फिरि पछिताना विरिध भयौ ॥
सूखे सरवर पालि बंधावै लुनें खेति हठि बारि करै ।
अयौ चोर तुरंगहिं लै गयौ मोहड़ी राहत मुग्ध फिरै ||2||
सीस चरन कर कंपन लागे नैंन नीरु असराल बहै ।
जिभ्या बचन सूध नहिं निकसै तब सुक्रित की बात कहै ॥3॥ इत्यादि ।
निरंजनी सम्प्रदाय की
पोथी में उपर्यक्त पद की पाँचवीं पंक्ति के 'सरवरि' (= सरोवर में ) के
स्थान पर 'तरवरि' ( = पेड़ पर ) पाठ मिलता है और 'गुरुग्रंथ साहब' में जो कबीर वाणी
का अत्यधिक श्रेष्ठ पाठ प्रदान करता है और अब तक की प्राप्त प्रतियों में कालक्रम
की दृष्टि से सर्वाधिक प्राचीन है, 'हठि बारि करे' के स्थान पर 'हथवारि करै' पाठ मिलता है।
पालि (सं.) तालाब के चारों ओर के ऊँचे कगार को कहते हैं, तुल. जायसी, पदमावत 60-6: 'पालि जाइ सब ठाढ़ी
भई।' इस प्रसंग में निरंजनी सम्पद्राय के 'तरवरि' पाठ की भ्रांति
स्पष्ट है। गुरुग्रंथसाहब के 'हथवारि' पाठ का भी यहाँ कोई
प्रसंग-सम्मत अर्थ नहीं निकलता। इसके विपरीत 'हठि बारि करै' जो अन्य प्रतियों
का पाठ है, का अर्थ है- हठात् रोक लगाता है; और यही इस प्रसंग
में उपयुक्त प्रतीत होता है। इसी प्रकार छठवीं तथा सातवीं पंक्तियों में तुरंगहिं, मोहड़ी, नैन, तथा असराल के स्थान पर
गुरुग्रंथ साहब में क्रमशः तुरंतह, मेरी, नैनी और असार पाठ
मिलते हैं जो भ्रमात्मक हैं। 'तुरंतह' पाठ ग्रहण करने से वाक्य
में कर्म का लोप हो जाता है, 'मेरी' पाठ ग्रहण करने से 'मेरी राखत' निरर्थक हो जाता
है; 'नैनी' स्पष्ट ही पंजाबी प्रभाव के कारण है और 'असराल' (= निरंतर) के स्थान
पर असार लिपिभ्रम के कारण हो गया है जिससे अर्थ का अपकर्ष होता है।
उपर्युक्त पाठ - विकृतियों के कारणों की खोज करने से उनका इतिहास भी स्पष्टतया दृष्टिगोचर होने लगता है। इनमें से अधिकांश विकृतियाँ ऐसी हैं जो यह संकेत करती हैं कि जिस प्रति पर इन पाठों को प्रस्तुत करने वाली प्रतियाँ आधारित हैं वह कदाचित् फारसी लिपि में थी। इस सम्भावना का सबसे सटीक उदाहरण उपर्युक्त पाठांतरों में गुरुग्रंथ साहब का 'हथवारि' पाठ है। पहले उर्दू में 'ते' के ऊपर एक पड़ी लकीर खींचकर 'टे' बनाते थे। यदि यह लकीर जल्दी में भूल से छूट जाए तो 'ठ' का सरलता से 'थ' हो जाता है। 'हठि बारि' से 'हथवारि' बन जाने का और कोई दूसरा समाधान हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार अन्य पाठांतरों की विकृतियों के कारण भी संतोषजनक रूप से ढूँढ़े जा सकते हैं।
इस प्रकार अनेक शाखाओं की
प्रतियों के आधार पर कार्य करने वाले सम्पादक के सम्मुख पर्याप्त सामग्री तथा साधन
उपलब्ध होने के कारण अनेक पाठ-पाठांतर अपना-अपना इतिहास स्वयं बताते हुए उपस्थित
हो जाते हैं और किंचित् विवेक से कार्य करने पर उनमें से उपयुक्त पाठ पुनर्निर्मित
कर लेना बहुत कठिन कार्य नहीं होता, जबकि किसी एक शाखा या
प्रति के पाठ पर आधारित रहने से उद्भट विद्वान् सम्पादक की दृष्टि भी सीमित रह
जाने के लिए विवश हो जाती है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि प्राचीन कृतियों के
सम्पादक के सम्मुख सम्पादनशास्त्र की सूक्ष्म तथा जटिल प्रक्रिया की समस्याएँ रहती
ही हैं, साथ ही पाठों का निर्णय करने में भी इतने प्रकार के विकल्प
आते हैं कि उनके सम्बन्ध में तनिक भी असावधानी से कार्य करने पर मार्गच्युत हो
जाने का भय लगा रहता है। इसीलिए कुछ भ्रांतियों का रह जाना असंभव नहीं है।