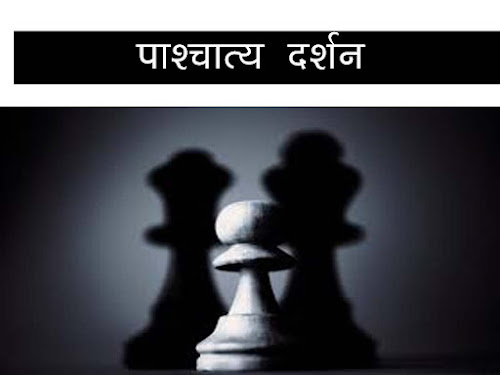पाश्चात्य दर्शन की भूमिका, दर्शनशास्त्र की सामाजिक प्रासंगिकता
पाश्चात्य दर्शन की भूमिका
- अपने दर्शन और सांस्कृतिक मूल्यों को आत्मसात करने के लिए अन्य दार्शनिक विचारधाराओं का सम्यक् बोध भी आवश्यक होता है। जो विचारक अन्य संस्कृतियों और जीवन-मूल्यों की उपेक्षा करते हैं, उनका अपना सांस्कृतिक मूल्य-बोध एकांगी तथा संकीर्ण हो जाता है। पाश्चात्य दर्शन के मूल तत्त्वों को बिना समझे हुए हमारी भारतीयता की पहचान भी अपूर्ण होगी। इसलिए विभिन्न पाश्चात्य दार्शनिकों के सिद्धांतों का विवेचन करते समय उनकी संक्षिप्त तुलना प्रासंगिक भारतीय दार्शनिकों के मतों से की गयी है। दार्शनिक अनुशीलन के प्रारम्भ से लेकर अर्वाचीन दर्शन तक ज्ञान, सत् और मूल्य अथवा सत्यं शिवं सुन्दरं का विवेचन और मूल्यांकन ही दार्शनिक चिन्तन का केन्द्र रहा है। केवल बीसवीं शताब्दी का विश्लेषी दर्शन इसका अपवाद है क्योंकि विश्लेषी दार्शनिकों की अभिरूचि परम्परागत दार्शनिक समस्याओं के निरूपण में नहीं थी। किन्तु प्रस्तुत पुस्तक में समसामयिक दर्शन की इस प्रवृत्ति का विवेचन नहीं हो सका है।
- आज की बदलती हुई वैश्वीकरण और उत्तर आधुनिक चिन्तन की परिस्थितियों में स्वयं दर्शनशास्त्र की सामाजिक प्रासंगिकता से सम्बन्धित प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। अतः किसी विशिष्ट दार्शनिक परम्परा का विवेचन करने से पूर्व स्वयं दार्शनिक अनुशीलन की सामाजिक प्रासंगिकता से सम्बन्धित प्रश्नों के विभिन्न पक्षों पर संक्षिप्त प्रकाश डालना आवश्यक हो जाता है।
दर्शनशास्त्र की सामाजिक प्रासंगिकता (The Social Relevance of Philosophy)
- मनुष्य का जीवन और चिन्तन दोनों साथ-साथ प्रारम्भ होता है। जब तक मनुष्य में चिंतन का विकास प्रारम्भ नहीं होता है तब तक वह सही अर्थों में मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं होता है। मनुष्य में यह जानने की स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि जीवन का क्या लक्ष्य है? मानव जीवन का क्या अर्थ है ? मानवेतर प्राणी न तो यह जानने का प्रयास करते हैं और न यह जानने में समर्थ हैं कि जीवन का क्या लक्ष्य है अथवा जीवन का क्या अर्थ है? इस जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए मानव अपने जीवन के लक्ष्यों एवं जीवन मूल्यों के प्रति अपना एक दृष्टिकोण विकसित कर लेता है। जीवन के स्वरूप और लक्ष्य को समझने के लिए जगत् के स्वरूप एवं प्रयोजन को समझना भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि मनुष्य का जीवन और मूल्यों का अनुसंधान इस जगत् में ही संभव होता है। अतः यह जगत् भी स्वाभाविक रूप से मानव-चिंतन का विषय हो जाता है।
- यदि जगत् के स्वरूप पर अनुशीलन किया जाय तो यह अत्यन्त विचित्र प्रतीत होता है। हम यह देखते हैं कि एक ओर बसन्त की सुषमा एवं मादकता समस्त प्राणियों को आहलादित करती है तो दूसरी ओ गरमी की तपन से वे व्याकुल हो जाते हैं। इसी प्रकार ऋतुओं का परिवर्तन, ऊपर तारों से भरा हुआ आकाश, भूकम्प, तूफान, महामारी, ज्वालामुखी विस्फोट आदि मनुष्य के मन में कौतूहल, भय, आश्चर्य एवं जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। वैज्ञानिक इन घटनाओं के स्वरूप की व्याख्या कारण कार्य नियम के आधार पर करते हैं । किन्तु कारण- कार्य श्री श्रृंखला का ज्ञान मानव - कौतूहल को शान्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कारण कार्य का सिद्धान्त केवल यह निर्दिष्ट करता है कि ये घटनाएँ किसी विशेष नियम के अनुसार घटित होती हैं। किन्तु विज्ञान यह नहीं स्पष्ट कर पाता है कि इस जगत् का क्या प्रयोजन है? ये घटनाएँ इस नियम के अनुसार क्यों घटित होती हैं? यही कारण है कि वैज्ञानिक ज्ञान के विकसित होने पर भी आज 21वीं शताब्दी में भी यह प्राकृतिक जगत् मनुष्य के लिए आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। यह ब्रह्माण्ड सौन्दर्य से युक्त ( Beautious) और उदात्त (Sublime) है। इसके समग्र स्वरूप को समझने की जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से मनुष्य को एक विशेष प्रकार के चिन्तन के लिए प्रेरित करती है। इसे फलस्वरूप दार्शनिक अनुशीलन का विकास होता है।
इस दृष्टि से चिन्तन की दो विधाएँ हो सकती हैं :
(1) समस्त विषय के स्वरूप को उसकी समग्रता में एक साथ जानने का प्रयास करना ।
(2) किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके प्रत्येक अंश को पृथक्-पृथक् जानने का प्रयास करना।
- इनमें से प्रथम पद्धति ही दार्शनिक चिंतन का आधार हो सकती है, जबकि दूसरी विधा का प्रयोग विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। दार्शनिकों ने ब्रह्माण्ड के स्वरूप का ज्ञान इसकी सम्पूर्णता में करने के लिए चिन्तन की प्रथम विधि का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त दार्शनिक पद्धति का बौद्धिक होना अनिवार्य है ताकि रोग-द्वेष आदि मनोविकारों से मुक्त होकर तत्त्व के स्वरूप का निष्पक्ष एवं तटस्थ दृष्टि से ज्ञान प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार परम्परागत रूप से दर्शनशास्त्र मनुष्य की अनुभूतियों का तार्किक विश्लेषण और मूल्यांकन करके यह निर्धारित करने का प्रयास करता है कि इस जीवन और जगत् (ब्रह्मांड ) का मूल आधार कोई तात्त्विक सत्ता है अथवा नहीं? दर्शनशास्त्र की यह अवधारणा मुख्य रूप से पाश्चात्य दर्शन के परिप्रेक्ष्य में की गयी है। यद्यपि भारतीय एवं पाश्चात्य दार्शनिकों की चिन्तन पद्धतियों एवं दृष्टिकोणों में कुछ मौलिक अन्तर है, तथापि दोनों दार्शनिक परम्पराओं में सम्पूर्ण ब्रह्मांड एवं उसके तात्त्विक आधार की खोज (तत्त्व - ज्ञान) को अपने अपने ढंग से दार्शनिक चिंतन का विषय माना गया है। सम्पूर्ण ब्रह्मांड को दार्शनिक चिंतन का विषय कहने का तात्पर्य यह है कि प्रायः दार्शनिक विश्व की व्यवस्था के संचालक आधारभूत, अर्थात् मौलिक (Foundational) नियमों की खोज करने का प्रयास करते रहे हैं।
- दर्शनशास्त्र के विरुद्ध प्रायः यह आक्षेप लगाया जाता है कि दार्शनिक प्रश्नों को कभी भी हल नहीं किया जा सकता है। इन प्रश्नों का अन्तिम समाधान प्राप्त करने के लिए हम कब तक प्रतीक्षा करते रहेंगे? किन्तु ऐसे आक्षेप दर्शनशास्त्र के साथ-साथ विज्ञान के क्षेत्र में भी लागू होते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में ऐसी अनेक समस्याएँ रही हैं, जिनका उत्तर बहुत बाद में मिला। यहाँ तक कि आज भी वैज्ञानिक ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर खोजने में लगे हुए हैं. जिनका संतोषप्रद उत्तर विज्ञान नहीं दे पा रहा है। यदि इन प्रश्नों को अनुत्तरणीय मान करके वैज्ञानिक उनकी खोज का प्रयास न करें तो विज्ञान की प्रगति ही अवरूद्ध हो जायेगी। गैलीलियो और न्यूटन के अनेक सिद्धांतों में परवर्ती वैज्ञानिकों ने संशोधन एवं परिमार्जन किया। इसके फलस्वरूप वैज्ञानिक अनुसंधान उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहा है। यही बाद दार्शनिक अनुसंधान के विषय में लागू होती है। यह अवश्य है कि दार्शनिक प्रश्नों का स्वरूप वैज्ञानिक प्रश्नों से भिन्न होता है। दार्शनिक समस्याएँ अत्यंत गंभीर, व्यापक एवं सार्वभौमिक प्रकृति की होती हैं। इसलिए उनका कोई सर्वमान्य एवं सबके द्वारा स्वीकृत उत्तर प्राप्त करना कठिन होता है। विश्व का स्वरूप और प्रयोजन क्या है? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई ? सत् क्या है? ज्ञान क्या है? ज्ञान, मूल्य और सत् में क्या सम्बन्ध है? ज्ञान और आचरण का आदर्श प्रतिमान क्या हो सकता है? इत्यादि । इस प्रकार के दार्शनिक प्रश्न अत्यंत जटिल, व्यापक एवं गहन चिन्तन की माँग करते हैं। ये प्रश्न भले ही कठिन और जटिल हों, परन्तु हम इसके बारे में सोचना बन्द नहीं कर सकते हैं। इन प्रश्नों के अनेक उत्तर दिये गये हैं और अभी अनेक उत्तर दिये जा सकते हैं। इन प्रश्नों के बारे में विभिन्न दार्शनिकों या दार्शनिक सम्प्रदायों के अपने अलग-अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक संस्कृति के अन्तर्गत मनुष्य की अपनी एक जीवन-पद्धति होती है। उसका ज्ञान, मूल्य एवं सत् के प्रति अपना एक दृष्टिकोण होता है। इस दृष्टिकोण और जीवन-पद्धति के अनुरूप ही मानव जीवन के समस्त कार्यक्रम निर्धारित होते हैं। अतः बुद्धिजीवियों के बीच में विवाद कुशल या अकुशल, सुसंगतिपूर्ण या विसंगतिग्रस्त दार्शनिक चिंतन, विचार पद्धति, तत्त्वमीमांसा, ज्ञानमीमांसा, मूल्यमीमांसा आदि के स्वरूप को लेकर हो सकता है। किन्तु कोई भी विचारशील मनुष्य दार्शनिक चिंतन से बच नहीं सकता है। वस्तुतः दार्शनिकों में सहमति अथवा असहमति का प्रश्न उतना महत्त्वपूर्ण नहीं होता है जितना कि चिन्तन-पद्धति का सामञ्जस्यपूर्ण होना महत्त्वपूर्ण है। वर्तमान युग में दार्शनिक अनुशीलन के प्रमुख बिन्दु क्या हो सकते हैं? आज के दबलते हुए परिवेश में, देश - काल एवं परिस्थिति के अनुरूप दार्शनिक चिंतन की दिशा क्या होनी चाहिए ? इन प्रश्नों पर दार्शनिकों में मतभेद हो सकता है। किन्तु इन प्रश्नों पर मतभेद होते हुए भी दार्शनिक चिन्तन समाज की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह अवश्य है कि दार्शनिक प्रश्नों को लेकर दार्शनिकों में विवाद होता रहता है। उनमें प्रायः असहमति पायी जाती है। इस संदर्भ में पश्चिम में एक समालोचक और दर्शनिक पी० ए० शिल्प का यह कथन उल्लेखनीय है- “ शायद ( इन गहन और व्यापक दार्शनिक प्रश्नों के स्वरूप को लेकर ) दर्शनिकों में असहमति होनी ही चाहिए। " किन्तु इस असहमति का कारण न तो दार्शनिकों का अज्ञान है और न उनका गहन चिन्तन में अकुशल एवं असमर्थ होना । इस असहमति का कारण दार्शनिक समस्याओं का बहुआयामी एवं जटिल होना है। इसके अतिरिक्त इन दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर मनुष्य की जीवन-शैली, उनकी सांस्कृतिक संरचना एवं उनके पृथक् पृथक् दृष्टिकोणों से प्रभावित होते हैं।
- वस्तुतः दर्शनिक विचारों में भिन्नता के कारण ही विभिन्न सम्प्रदायों की जीवन-शैली अलग-अलग होती है। इस जीवन शैली एवं विचार पद्धति के अनुरूप ही मनुष्य के समस्त कार्यक्रमों का निर्धारण होता है। यही कारण है कि हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक मूल्यों का स्वरूप और संरचना दार्शनिक अनुशीलन से प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, ईश्वर के अस्तित्व के बारे में भिन्न-भिन्न मत रखने वाले व्यक्तियों की जीवन-पद्धति एक-दूसरे से अलग होती है। यही बात व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के संदर्भ में लागू होती है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान होती हैं उसके दार्शनिक चिन्तन का भी अपना एक अलग ढाद्दचा (मॉडल) होता है। हमारी जीवन-पद्धति, मूल्यबोध, आचरण, लोक कल्याण के प्रतिमान, अर्थव्यवस्था, राजनीति की प्रणालियाँ आदि हमारी दार्शनिक सोच ( विचारधारा) से प्रभावित होती हैं। किसी सैद्धांतिक आधार के बिना मानव जीवन, पर्यावरण, राजनीति, समाज-नीति एवं आर्थिक नीति अस्त-व्यस्त हो जाती ही। इन सब को सुव्यवस्थित, संतुलित एवं परस्पर सामञ्जस्यपूर्ण बनाने के लिए जिस आधारभूमि एवं सिद्धांत की आवश्यकता होती है, वह दर्शनशास्त्र से प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट है कि दार्शनिक प्रश्न कोरे अमूर्त चिंतन पर आधारित कल्पना नहीं हैं। ये प्रश्न मानव जीवन की आवश्यकताओं से उत्पन्न होते हैं और जीवन एवं जगत् को सुव्यवस्थित आहलादक एवं कल्याणकारी बनाने के सूत्र हैं। इन प्रश्नों के उत्तर देने के प्रयत्न में ही अनेक दार्शनिक सिद्धांतों (जेसे-तत्त्वमीमांसीय, ज्ञानमीमांसीय, मूल्यमीमांसीय इत्यादि) का प्रतिपादन किया गया है।
- दार्शनिक प्रश्नों के विरुद्ध एक आक्षेप यह है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक इन प्रश्नों का कोई एक सुनिश्चित उत्तर नहीं दिया जा सका है। दर्शनशास्त्र अपनी परम्परागत ( घिसी-पिटी ) पुरानी समस्याओं तक ही सीमित है। ये समस्याएँ भविष्य में भी इसी प्रकार बनी रहेंगी। उनका कोई समुचित समाधान संभव न हो सकेगा। इस प्रकार दार्शनिक चिंतन के क्षेत्र में नवीनता का अभाव है। इन पर विचार करने से क्या लाभ है?
- वस्तुत: यह आक्षेप दर्शनशास्त्र के इतिहास की गलत समझ के कारण किया जाता है। यह कहना सत्य नहीं है कि दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर देने में कोई सफलता नहीं मिली है। सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन होने के साथ-साथ दार्शनिक समस्याओं के प्रति मनुष्य के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होता रहता है। आधुनिक युग का मानव दार्शनिक प्रश्नों को अपने पूर्वजों की अपेक्षा अधिक अच्छे ढंग से समझता है। ये प्रश्न भले ही अभी तक हल नहीं हुए हैं, परन्तु आज के उत्तर पहले दिये गये उत्तरों की अपेक्षा अधिक तर्कसंगत, परिमार्जित एवं विकसित हैं। दार्शनिक समस्याओं के विषय में हमारी समझ प्राचीन काल के मनुष्यों की तुलना में अधिक परिपक्व और विकसित हुई है। दार्शनिक समस्याएँ भले ही प्राचीन हों, परंतु उनके प्रति विभिन्न युगों में दार्शनिकों के दृष्टिकोण नवीन होते हैं। सच तो यह है कि प्राचीन समस्याओं के प्रति नवीन दृष्टि एवं नवीन व्याख्याएँ, ही दार्शनिक चिन्तन को मौलिकता प्रदान करती हैं। इस प्रकार दार्शनिक चिन्तन समाज, साहितय, धर्म और विज्ञान के घात-प्रतिघात से विकसित होता है। यही कारण है कि प्रत्येक युग में दार्शनिक समस्याओं के नवीन आयाम विकसित होते रहते हैं। जिस प्रकार साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, अर्थात् जिस प्रकार युग के अनुरूप नवीन साहित्यिक दृष्टि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार समय परिवर्तन के साथ-साथ प्रत्येक संस्कृति के मार्गदर्शन के लिए दार्शनिक चिन्तन की भी आवश्यकता होती है। अतः यह कहना तर्कसंगत नहीं है कि दर्शनशास्त्र के प्रारम्भ से लेकर आज तक दार्शनिक समस्याओं के स्वरूप में कोई नवीनता नहीं है।
- जीवन और जगत् के प्रति हमारा चिन्तन जितना अधिक व्यवस्थित ( Systematic ) और सामंजस्यपूर्ण होगा, वह उतना ही अधिक संतुलित एवं सफल होगा। किसी दार्शनिक की सफलता अपने ज्ञान एवं विचारों को जीवन में आत्मसात् करने में निहित होती है । दार्शनिक भले ही स्वयं कोई आन्दोलन और क्रान्ति न कर सकें, परन्तु उनके विचार किसी न किसी समाज-सुधारक अथवा राजनीतिज्ञ को माध्यम बनाकर आन्दोलन का रूप धारण कर लेते हैं। कोई भी क्रान्ति अथवा आंदोलन समाज में घटित होने के पूर्व मनुष्य के विचारों में जन्म लेता है। क्रान्तिकारी विचार किसी न किसी दार्शनिक दृष्टि पर आधारित होने पर ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करते हैं। जैसे- उदाहरण के लिए कार्ल मार्क्स के विचारों ने लेनिन को प्रभावित किया। उसके फलस्वरूप उसने अपने समय के रूसी समाज को व्यवस्थित एवं संगठित करने का महान कार्य सम्पन्न किया। स्वयं मार्क्स का द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हेगल एवं फ्वेरबाक (Feuerbach) के विचारों से प्रभावित हुआ था। इसी प्रकार पश्चिम में सुकरात, प्लेटो, अरस्तू, कांट, रूसो इत्यादि एवं भारत में महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, आदि शंकराचार्य, कौटिल्य, स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गांधी आदि के दृष्टान्त विद्यमान हैं। इन विचारकों ने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से समाज, धर्म और राजनीति को प्रभावित किया।
- उत्तर आधुनिकता (Post Modernity ) से प्रभावित कुछ विचारकों एवं समालोचकों के अनुसार आधुनिक दार्शनिक चिन्तन ज्ञान, सत् और मूल्य के जिन निरपेक्ष, सार्वभौम और सर्वग्राह्यमानदण्डों की खोज करने का प्रयास कर रहा है, वे संभव ही नहीं हैं क्योंकि सत्ता का कोई निरपेक्ष एवं सार्वभौम ज्ञान नहीं हो सकता है। ज्ञान के प्रामाण्य (वैधता) के सार्वभौम नियम संभव नहीं हैं। इसी प्रकार कोई निरपेक्ष मूल्य भी नहीं है। अतः दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में सार्वभौमिकता, तार्किक सुसंगति और सत्य की खोज करने का प्रयास निरर्थ है । इस दृष्टि से ज्ञान, सत् और मूल खण्डित, बहुवचनीय और देश-काल एवं परिस्थिति -सापेक्ष है।
- प्रस्तुत संदर्भ में उत्तर आधुनिकतावाद की व्याख्या एवं मूल्यांकन करना विषयान्तर होगा। किन्तु यहाँ यह कहना प्रासंगिक होगा कि इस विचारधारा से प्रभावित विचारकों को अपने मतों की स्थापना के लिए किसी न किसी मानदण्ड अथवा प्रतिमान को अवश्य अपनाना पड़ेगा। ज्ञान, मूल्य और सत् की कोई ओचना किसी न किसी मानदंड के आधार पर ही की जा सकती है। यदि बिना किसी मानक के दर्शनशास्त्र की आलोचना की जाती है तो उसे सारगर्भित और युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता हैं इसके विपरीत यदि दार्शनिक समस्याओं का खंडन करने के लिए कोई मानदंड प्रयुक्त किया जाता है तो निश्चित रूप से वह किसी न किसी दार्शनिक विचारधारा पर ही आधारित होगा। अतः किसी विशेष प्रकार की दार्शनिक पद्धति एवं दार्शनिक विचारधारा के निराकरण को सम्पूर्ण दर्शन का निराकरण नहीं कहा जा सकता है।
- कुछ आलोचकों के अनुसार दर्शनशास्त्र अव्यावहारिक होता है। यह दृष्टिकोण साधारण लोगों की सतही सोच पर आधारित है। दार्शनिक चिंतन के प्रति उनकी गलत समझ को दूर करने की आवयकता है। किसी दार्शनिक विचारधारा से सहमत होना आवा असहमत होना एक अलग बात हैं, परन्तु दर्शनशास्त्र मात्र को निरर्थक, अव्यावहारिक एवं अनुपयोगी कहना दर्शन के प्रति एक भ्रामक दृष्टिकोण पर आधारित है। क्या व्यावहारिक होने का अर्थ बिना किसी सिद्धांत के अपने संवेगों, भवनाओं एवं वासनाओं के वशीभूत होकर आचरण करना है? क्या व्यावहारिक होने का अर्थ अवसरवादी एवं चापलूस होना है? वास्तव में 'व्यावहारिक होने के नाम पर अवसरवादी, कुतर्क वितंडा और चापलूसी को गलत प्रोतसाहन देना व्यवहार और दर्शनशास्त्र दोनों की गलत समझ है। मनुष्य के व्यावहारिक होने का निहितार्थ यह है कि जीवन की वास्तविकताओं (Grand Realities) को ध्यान में रखकर उनके अनुरूप व्यक्ति एवं समाज के कल्याण की दिशा निर्धारित की जाय। इसके लिए तार्किक एवं मूल्यपरक दृष्टिकोण को विकसित करने की आवश्यकता है जो बिना किसी दार्शनिक चिंतन प्रणाली के संभव नहीं हो सकता है।
- कुछ आलोचकों का यह कहना है कि आज का युग अर्थ-प्रधान है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं कम्प्यूटर के इस युग में मनुष्य की प्रमुख आवश्यकता जीविकोपार्जन के साधन सुलभ कराना है। ऐसी परिसिति में दर्शनशास्त्र की क्या उपयोगिता हो सकती है? इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ एक अन्य प्रश्न यह है कि क्या मनुष्य के जीवन का अन्तिम लक्ष्य जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराना है? यह सत्य है कि अर्थोपार्जन मानव की जीविका के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। किन्तु यह मानव जीवन का अन्तिम लक्ष्य नहीं है। दर्शनशास्त्र का सम्बन्ध भले ही प्रतयक्ष रूप से जीविकोपार्जन न हो, परन्तु इसका प्रयोजन जीविकोपार्जन के लक्ष्य को निर्धारित करना है। दूसरे शब्दों में, जीविकोपार्जन मनुष्य की एक मूलभूत आवश्यकता है, परन्तु यह अपने आप मे साध्य नहीं है। यह किसी उच्चतर साध्य की प्राप्ति का साधन मात्र है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अर्थोपार्जन आदि मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिए साधन- मूल्य हैं। उनका लक्ष्य कतिपय साध्यमूल्यों की प्राप्ति है। मानव जीवन का परम आदर्श, निः श्रेयस एवं अन्तिम लक्ष्य क्या है ? दार्शनिक अनुशीलन इसी का बोध कराता है। यह जीविका भले न प्रदान कर सके, परन्तु जीवन के यथार्थ स्वरूप एवं लक्ष्य का मार्ग दर्शक है। कोई भी संवेदनशील एवं बुद्धिजीवी मनुष्य केवल खाने के लिए (जीविकोपार्जन हेतु ) जीवित नहीं रहना चाहता है, बलिक जीवन में कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जीवित रहना चाहता है, बल्कि जीवन में कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जीवित रहना चाहता है। अतिशय भोगवाद एवं सुखवाद की आलोचना करते हुए जे०एस० मिल ने कहा है कि 'एक असंतुष्ट सुकरात होना एक संतुष्ट शूकर (Pig ) होने की अपेक्षा अधिक श्रेयस्कर है।' असंतुष्ट ज्ञानी एवं दार्शनिक होना एक संतुष्ट मूर्ख होने से अच्छा है। कोई मूर्ख व्यक्ति अपने को अधिक सुखी या धन्य समझता है। तो इसका कारण यह है कि वह (मूर्ख) केवल अपने ही दृष्टिकोण को समझता है। इसके विपरीत दार्शनिक दोनों के दृष्टिकोणों (अर्थात् ) व्यष्टि एवं समष्टि दोनों के दृष्टिकोणों) को जानता है। इससे स्पष्ट है कि दर्शनशास्त्र ऐसे मूल्यों, आदर्शों एवं निःश्रेयस से सम्बन्धित है जो मनुष्य को सदैव मनुष्य बने रहने के लिए प्रेरित करते हैं। जब तक मनुष्य की चिंतन-पद्धति सन्तुलित, मूल्यपरक और निष्पक्ष नहीं होगी तब तक हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी से प्राप्त संसाधनों का सुदपयोग लोक कल्याण की दिशा में नहीं कर सकते हैं। आधुनिक युग संकट का युग है। विश्व के विभिन्न भागों में व्याप्त हिंसा, तनाव, आतंकवाद, धार्मिक एवं जातीय संघर्ष, नशाखोरी, भ्रष्टाचार एवं अन्य सामाजिक बुराइयाँ केवल विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं कम्प्यूटर से दूर नहीं की जा सकती हैं। इनसे बचने के लिए व्यवस्थित विचार पद्धति एवं मूल्यपरक शिक्षा के द्वारा मनुष्य की सोच को, जीवन-दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। जब- जब मानव समाज सांस्कृतिक क्षरण की त्रासदी से गुजरता है, तब-तब दार्शनिक अनुशीलन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। वस्तुत: दार्शनिक प्रक्रिया एक सामाजिक प्रक्रिया है। दार्शनिक दृष्टि से रहित समाज एक असभ्य, बर्बन एवं आदिम समाज ( Primitive Society) होगा। प्राय: ऐसा समाज दिशाहीन, लक्ष्यहीन एवं अदूरदर्शी मनुष्यों की एक भीड़ के समान होता है। दर्शनशास्त्र समाज की प्रज्ञा चक्षु है और प्रज्ञा समाज की गतिशील आत्मा है। दर्शनशास्त्र का उद्भव एवं विकास समाज में होता है। उस पर सामाजिक मान्यताओं, भाषा, धर्म, संसकृति आदि का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक होता है। हम दर्शनशास्त्र और समाज की एक-दूसरे से पृथक् रूप में कल्पना नहीं कर सकते हैं, अर्थात् दोनों में अवियोज्य सम्बन्ध है। यह प्रश्न करना कि दर्शनशास्त्र की समाज के लिए क्या प्रासंगिकता है, एक अप्रासंगिक प्रश्न है। दार्शनिक चिन्तन की सामाजिक प्रासंगिकता दर्शनशास्त्र का एक अवियोज्य आयाम है।
- यदि कोई दर्शन समाज की सृजनात्मक आत्मा, अर्थात् समाज की जमीनी वास्तविकताओं, मूल्यों एवं संस्कृति की उपेक्षा करता है तो वह अप्रासंगिक हो जाता है। वह समाज के लिए ग्राह्य नहीं रह जाता है। इसके अतिरिक्त यदि दार्शनिक चिंतन को अभिव्यक्त करने वाली भाषा मृतप्राय हो जाती है तो दर्शनशास्त्र समाज को प्रभावित नहीं कर पाता है। इसके फलस्वरूप वह समाज के लिए अप्रासंगिक हो जाता है। उदाहरण के लिए आधुनिक यूरोपीय समाज के लिए लैटिन भाषा में अभिव्यक्त दर्शन और आज के भारतीय समाज के लिए संस्कृत, पाली एवं प्राकृत भाषा में व्यक्त दर्शन अप्रासंगिक हो जायेगा। इसी प्रकार किसी भी विदेशी भाषा में व्यक्त स्वदेशी दर्शन उस देशीय समाज के लिए दुर्बोध हो जाता है। वस्तुतः किसी भी राष्ट्र के दर्शन की अभिव्यक्ति उसकी अपनी भाषा में होना चाहिए। यदि किसी दार्शनिक विचारधारा को व्यक्त करने वाली भाषा समाज के जनमानस के लिए अपिरिचित हो तो ऐसा दार्शनिक चिन्तन समाज से दूर हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई विचारधारा सामाजिक प्रगति, वैचारिक स्वतंत्रता आदि मूल्यों को बाधित करती है तो वह समाज के लिए न केवल अप्रासंगिक हो जाती है, बल्कि बहुत ही घातक ( खतरनाक ) हो जाती है। उदाहरण के लिए, शास्त्रीय ईसाई दर्शन ( कैथोलिक सम्प्रदाय की कट्टरपंथी विचारधारा) आधुनिक यूरोपीय दर्शन के विकास के पूर्व बहुत घातक सिद्ध हुआ। अनेक वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को कठोर यातनाएँ दी गयीं। इससे सामाजिक प्रगति एवं वैचारिक स्वतंत्रता कुण्ठित हुई। किन्तु यह उल्लेखनीय है कि किसी दार्शनिक विचारधारा के विकास, सामाजिक प्रासंगिकता और सृजनात्मकता के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं। इनमें से प्रथम शर्त यह है कि दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति राष्ट्र भाषा और साधारण भाषा में होनी चहिए। यदि दार्शनिक चिंतन को अभिव्यक्त करने वाली भाषा सुबोध न हो तो ऐसा दर्शन सरलतापूर्वक ग्राह्य न होने के कारण समाज की मुख्य धारा से कट जाता है। इसके अतिरिक्त किसी दार्शनिक आदर्श को जीवन्त और सृजनशील (Creative) बनाये रखने के लिए दार्शनिक वाद-विवाद के फलस्वरूप 'असहमति के प्रति सद्भाव' का होना आवश्यक है। बौद्धिक सहनशीलता (Intellectual Tolerance) और आत्मलोचन (Self-Criticism) की प्रवृत्ति के अभाव में कोई दर्शनशास्त्र न तो समाज के लिए प्रासंगिक हो सकता है और न चिरस्थायी हो सकता है। वस्तुतः बौद्धिक सहनशीलता एवं आत्मालोचन की प्रवृत्ति से वंचित दार्शनिक विचारधाराएँ फासीवाद एवं नस्लवाद को अनुचित रूप से प्रोतसाहित करती रहती हैं। इससे दर्शनशास्त्र के अपने लक्ष्य से विचलित होने का भय (खतरा ) रहता है। अपने से विपरीत ( विरोधी ) मतों के प्रति सद्भाव, शाश्वत संवाद एवं वाद-विवाद तथा समन्वय की प्रक्रिया से प्रतयेक जीवन्त दार्शनिक सम्प्रदाय अपना पुनर्मूल्यांकन और अपने सिद्धांतों की पुनर्संरचना (Reconstruction) आवा पुनर्गठन करता रहता है। में उसकी सामाजिक प्रासंगिकता निहित होती है।
- कुद विचारकों के अनुसार दर्शनशास्त्र की सामाजिक प्रासंगिकता दर्शन का न तो साध्य हैं और न सर्वस्व है क्योंकि विश्व में न तो कोई सार्वभौमिक समाज है और न कोई सार्वभौम दर्शनशास्त्र है। यह सच है कि विश्व में अनेक समाज एवं अनेक प्रकार की दार्शनिक प्रवृत्तियाँ हैं। जो दर्शनशास्त्र किसी विशेष देश-काल एवं परिसिीति में एक समाज के लिए प्रासंगिक हैं, हो सकता है कि अन्य परिस्थितियों में एवं अन्य समाजों के लिए सार्थक और उपयोगी न हो। किन्तु विश्व में अनेक समाजों एवं संस्कृतियों का होना कोई समस्या नहीं है। प्रतयेक समाज की अपनी अलग-अलग दार्शनिक एवं सांस्कृतिक मान्यताएँ, विचार एवं मूल्यबोध हो सकता है। इससे सिद्ध होता है कि समाज और दर्शनशास्त्र एक-दूसरे को तर्कतः प्रतिपन्न करते हैं। अतः दर्शनशास्त्र की सामाजिक प्रासंगिकता उसका एक अवियोज्य आयाम है।
- आज के बदलते हुए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवेश में दार्शनिकों का यह दायित्व है कि वे अपने विचारों और सिद्धांतों से समाज की चिन्तन प्रणाली (सोचने के तरीके) को परिमार्जित करें। समाज के व्यावहारिक प्रश्नों का समाधान खोजने की आवश्यकता है। उन्नीसवीं शताब्दी के महान विचारक कार्ल मार्क्स ने अपने युग के दार्शनिकों के आचरण पर क्षोभ व्यक्त करते हुए यह चेतावनी दिया- ' दार्शनिकों का कार्य है संसार (समाज) को बदलना', अर्थात् शोषण मुक्त समाज की सीपना के लिए प्रयत्न करना । दर्शनिकों का कार्य केवल अनुशीलन ही नहीं, बल्कि उन्हें समाज को बदलने का प्रयत्न भी करना चाहिए। दर्शनशास्त्र की एक प्रमुख उपलब्धि बुद्धि के परिमार्जन के फलस्वरूप मनुष्य को व्यवस्थित एवं युक्तिसंगत चिंतन के योग्य बनाना है। मनुष्य के जीवन की अधिकांश सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक समस्याएँ अव्यवस्थित, अतार्किक, संकुचित एवं स्वार्थपरक दृष्टि के कारण पैदा होती हैं। यदि दर्शन की इस पद्धति का उपयोग पूर्वोक्त समस्याओं को हल करने के लिए अपनाया जाय तो विश्व की अनेक समस्याएँ स्वतः हल हो सकती हैं। साम्प्रदायिक एवं जातीय उन्माद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, अपराध आदि से सम्बन्धित समस्याएँ केवल विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं कम्प्यूटर के द्वारा दूर नहीं की जा सकती हैं। इन कुरीतियों को दूर करने के लिए समाज की मानसिकता (सामाजिक सोच) में परिवर्तन अथवा विचार प्रणाली में परिमार्जन की महती आवश्यकता है। इसके लिए दर्शनशास्त्र की तार्किक पद्धति एवं मूल्यात्मक दृष्टि (Evaluative Vision) की उपयोगिता और प्रासंगिकता से इन्कार नहीं किया जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर खोजने की जिज्ञासा मनुष्य के लिए स्वाभाविक होती है। मनुष्य की यह एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है कि वह अपने यथार्थ जीवन और अपनी सीमाओं से प्रायः संतुष्ट नहीं रहता हैं उसके मन में अपनी सीमाओं से परे 'जो कुछ है', उसके बारे में जानने की एक 'अदम्य इच्छा-शक्ति' (Nisus of Whole) पायी जाती है। कुछ विचारकों ने इसे मनुष्य में पायी जाने वाली 'स्वातिक्रमण' (Self Transcendence) की प्रवृत्ति कहा है। मनुष्य के पास 'जो कुछ है', वह उससे संतुष्ट नहीं होता है। यदि कोई मनुष्य अपने यथार्थ से संतुष्ट हो जाता है तो वह या तो देवत्व को प्राप्त कर लेता है अथवा विचारशून्य पशुओं की श्रेणी (कोटि) में सम्मिलित हो जाता है। किन्तु ये दोनों विकल्प मानव-जीवन एवं संस्कृति की प्रगति के लिए उपयुक्त नहीं हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और दार्शनिक अनुशीलन एक सामाजिक व्यापार है। दर्शनशास्त्र का इतिहास एक प्रकार से सामाजिक संस्कृति के इतिहास की ही मुख्य धारा है। अतः कोई संवेदनशील और जागरूक बुद्धिजीवी दार्शनिक चिंतन की उपेक्षा नहीं कर सकता है। वस्तुतः दार्शनिक प्रश्नों की उपेक्षा करना अथवा इन प्रश्नों को जटिल और कठिन होने के कारण टाल देना एक प्रकार का बौद्धिक पलायनवाद है। इससे स्पष्ट है कि दार्शनिक अनुशीलन प्रत्येक सुसंस्कारित समाज का स्वाभाविक व्यापार है। अतः समाज के लिए दर्शनशास्त्र की उपयोगिता और प्रासंगिकता से सम्बन्धित प्रश्न बहुत प्रासंगिक नहीं है।